

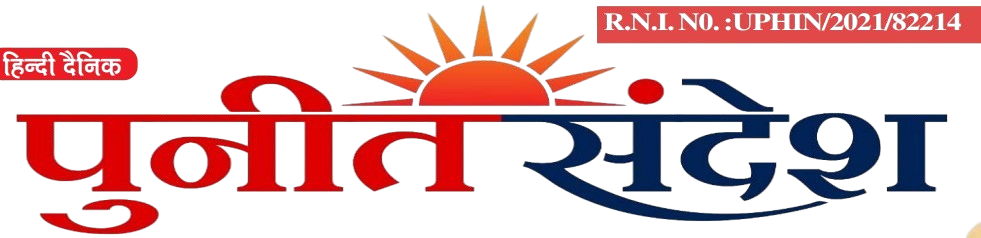



संहार का मूर्धन्य होना: सभ्यता के बोध पर प्रश्नचिन्ह

जब विनाश को सम्मान मिलने लगे, जब विध्वंस नीतियों के शिखर पर आसीन हो जाए और जब सौजन्यता दुर्बलता समझी जाने लगे — तब किसी भी सभ्यता के मूल में एक गंभीर दरार उत्पन्न हो जाती है। यही चेतावनी इस चिंतन से उभरती है कि यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ इसी दिशा में चलती रहीं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब संसार केवल बाह्य रूप से बचेगा, परंतु भीतर से पूर्णतः शून्य हो जाएगा।
विनाश का महिमामंडन: एक आत्मघाती प्रवृत्ति
इतिहास गवाह है कि जब-जब संहार को महत्ता मिली है, जब नष्ट करने की क्षमता को प्रगति का प्रतीक मान लिया गया है, तब-तब मानवता ने अपनी आत्मा को खो दिया है। आधुनिक विश्व में तकनीकी, सैन्य और आर्थिक वर्चस्व की होड़ में मानवीय मूल्य, करुणा और सौजन्य जैसे शब्द हाशिये पर चले गए हैं। और यदि यही क्रम चलता रहा, तो कोई भी उपलब्धि अंततः खोखली ही सिद्ध होगी।
नश्वरता के चारों ओर अनन्तता का भ्रम
हम जिन चीजों को स्थायी मान बैठते हैं — जैसे सत्ता, समृद्धि, संसाधन — वे सभी नश्वर हैं। जब चारों ओर क्षणभंगुरता ही व्याप्त है, तो क्या कोई भी उपलब्धि वास्तव में 'धन्य' बना सकती है? आत्मा के स्तर पर सोचें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य सफलता का आभास केवल अस्थायी है। यदि मनुष्य की अंतर्मन की शांति, आत्मीयता और परस्पर संबंध ही समाप्त हो जाएँ, तो क्या वास्तव में कोई भी उन्नति सार्थक रह जाती है?

विध्वंसक प्रवृत्तियाँ और संबंधों का विघटन
आज की वैश्विक राजनीति, सामाजिक संवाद और व्यक्तिगत व्यवहार में यह देखा जा सकता है कि असहमति अब विरोध नहीं बल्कि वैर बन चुकी है। जो किसी समय सहचरी शक्ति बन सकते थे, वे आज एक-दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर चुके हैं। प्रतिपार्श्विक (complementary) बनने के स्थान पर प्रतिस्पर्धा और प्रतिहिंसा की भावना ने स्थान ले लिया है। जब संबंध स्वार्थ और आक्रोश से संचालित हों, तो उनका अनन्य और अभिन्न रहना असंभव हो जाता है।
विश्वबोध की सीमाएँ और सभ्यता का भविष्य
जब चेतना ही संकीर्ण हो जाए, और ज्ञान के स्थान पर घृणा का प्रसार हो — तब वैश्विक बोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता। विश्व को चिरंतन मानने की हमारी धारणा तब चूर-चूर हो जाती है, जब हम उसे निरंतर आत्मघाती प्रवृत्तियों की ओर धकेलते हैं। यह संसार तब सनातन नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा मंच बन जाता है जहाँ शून्यता की पुनरावृत्ति ही नियति बन जाती है।
निष्कर्ष: चेतना की अंतिम पुकार
इस चिंतन का उद्देश्य केवल एक भावनात्मक उद्वेलन नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक और मानवीय चेतावनी है। जब संहार को मूर्धन्य बना दिया जाता है, तो बोध — जो किसी भी सभ्यता की आत्मा होता है — वह अपने ही मौन में विलीन हो जाता है।
हमें यह सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि सौजन्यता, करुणा, संयम और सह-अस्तित्व को हम पुनः केंद्र में नहीं लाते, तो वह दिन दूर नहीं जब बाह्य रूप से सजी-संवरी यह दुनिया भीतर से पूर्णतः शून्य और निर्वात बन जाएगी — एक ऐसा संसार, जो सनातन होने का दावा करेगा, परंतु उसके भीतर जीवन का कोई स्पंदन नहीं होगा।
अंकित राठौड़
Created On: June 16, 2025
















