

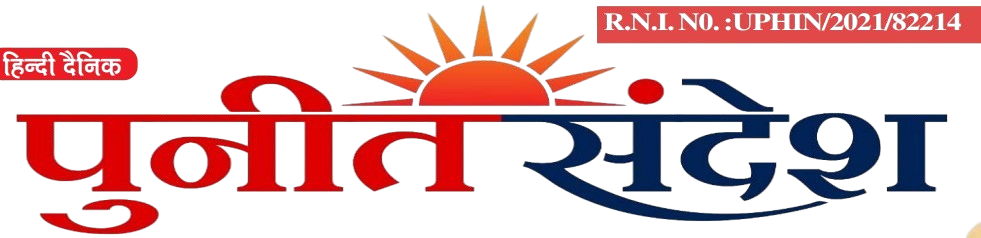



"कुम्भ-कथा : अमृत-मंथन व पर्व-प्रतिष्ठा की गाथा"

कुम्भ-कथा कुम्भ पर्व के इतिहास व दर्शन को सँजोने व साधने की कोशिश है। हर विवेचन कुछ विश्लेषण होता है और कुछ संश्लेषण। यह उचित भी है कि तथ्य व अवधारणा दोनों सहचर बन चलें, अन्यथा केवल सूचनात्मक विवरण का भी क्या रस!
कुम्भ-कथा मिथकों, कथाओं व प्रतीकों से होकर आगे बढ़ती है। हर मिथक, हर कथा कोई प्रतीक या भिन्न निहितार्थ लिए हुए है। इसकी भी अनेक परतें हैं। सबकी अपनी व्याख्याएँ भी। बस कहें, तो हर गल्प कपोल-कल्पना है। सुनें, गुनें, तो हर कथा में कल्पपर्यंत आयाम हैं। सबके अपने रस, सबकी अपनी विविधा।
यह कुम्भपर्व अमृतपर्व भी है, क्योंकि उसी के छलकने की तो कथा है। संसार में अमृत कहीं नहीं छलकता। अमृत एक ही है— आत्मा। लेकिन आत्मा का बोध कराने वाली विधा या उस बोधि का उपदेश भी तो अमृत उपदेश हो सकता है। पुराणों व किंवदंतियों में शिव द्वारा अमरकथा कहने की कथा है। महामुनि शुकदेव के जन्म की कथा ऐसे ही जुड़ी है। ये शुक भी क्या आत्मा या प्राण पखेरू के प्रतीक न होंगे?
धन्वन्तरि के साथ अमृत के उद्भव की कथा है। धन्वन्तरि का अर्थ धन से नहीं जुड़ा, मरुस्थल से जुड़ा है। धन्व शब्द मरु का पर्याय रहा है, वेदों में भी। तो धन्वन्तरि या तो मरुमरीचिका से जुड़ सकते हैं या मरुतृषा की तृप्ति से या फिर दोनों से। अमृत का संधान भी तो वही है, वह मृषा मरीचिका भी है और तृषा की तृप्ति भी है।
कुम्भपर्व की इस पौराणिक आख्यानपरक व्याख्या के साथ-साथ इसका खगोलवैज्ञानिक आधार भी समानांतर रूप में चलता रहता है, क्योंकि ग्रहों की विशेष स्थितियाँ ही कुम्भपर्व के काल का निर्धारण करती है। उनमें भी विशेषरूप से सूर्य, गुरु तथा चन्द्र का विभिन्न राशियों में संक्रमण ही कुम्भपर्व का नियामक होता है। सो इनमें उनको भी कई कथाओं में सम्मिलित कर लिया गया। सरल जन मन को ऐसे ही तो समझाया जा सकता है। हर ग्रह की विशिष्टता को बताने के लिए कोई रुचिर कथा रच ली गई। सूर्य सप्ताश्वरथी क्यों? चन्द्र रोहिणीप्रिय क्यों? शनि शनैश्चर क्यों? बृहस्पति गुरु क्यों? मंगल भौम क्यों? शुक्र दैत्यगुरु क्यों? पृथ्वी शेषासीन क्यों अंतस् में कूर्माधिष्ठित क्यों? ऐसे असंख्य प्रौढ प्रश्नों का उत्तर ये कथाएँ अपनी बालसुलभ शैली में दे देती हैं।

कुम्भपर्व का एक केंद्र सरिता-संगम है। दूसरा आयाम ग्रहयुति है। उसका तीसरा व वृहत्तर आयाम जनसमुदाय है, क्योंकि मेला ही तो है। चौथा आयाम संतसमाज है, क्योंकि उनका ही तो नेतृत्व है। पाँचवाँ आयाम संत-समन्वय है, क्योंकि यह संतों का भी परस्पर अधिवेशन है। छठा आयाम जनसामान्य का संत साक्षात्कार है, क्योंकि यह उनका सत्संग है। सातवाँ आयाम जनसामान्य का सामान्यीकरण है, क्योंकि यह क्षेत्रीयता से परे राष्ट्रीय व वैश्विक सम्मिलन है। वह हज या उमरा नहीं, वह उर्स नहीं, जेहाद नहीं। सर्वसमन्वय ही उसका स्वरूप है, वह उसका महत्तम व्यावहारिक उद्देश्य है। कोई जाति-पाँति का भेद नहीं। कोई पंडा-पुरोहित नहीं। सबको अपनी कथा कहने व सुनने का अधिकार है। कुछ स्नान कर निर्मल हुए, कुछ दान कर नि:स्व हुए। यहाँ हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। बस हमारे तुम्हारे बीच यह संगम। चिरंतन व सनातन। इसी के साथ शुभारंभ, इसी के साथ समापन।
Created On: March 01, 2025



























